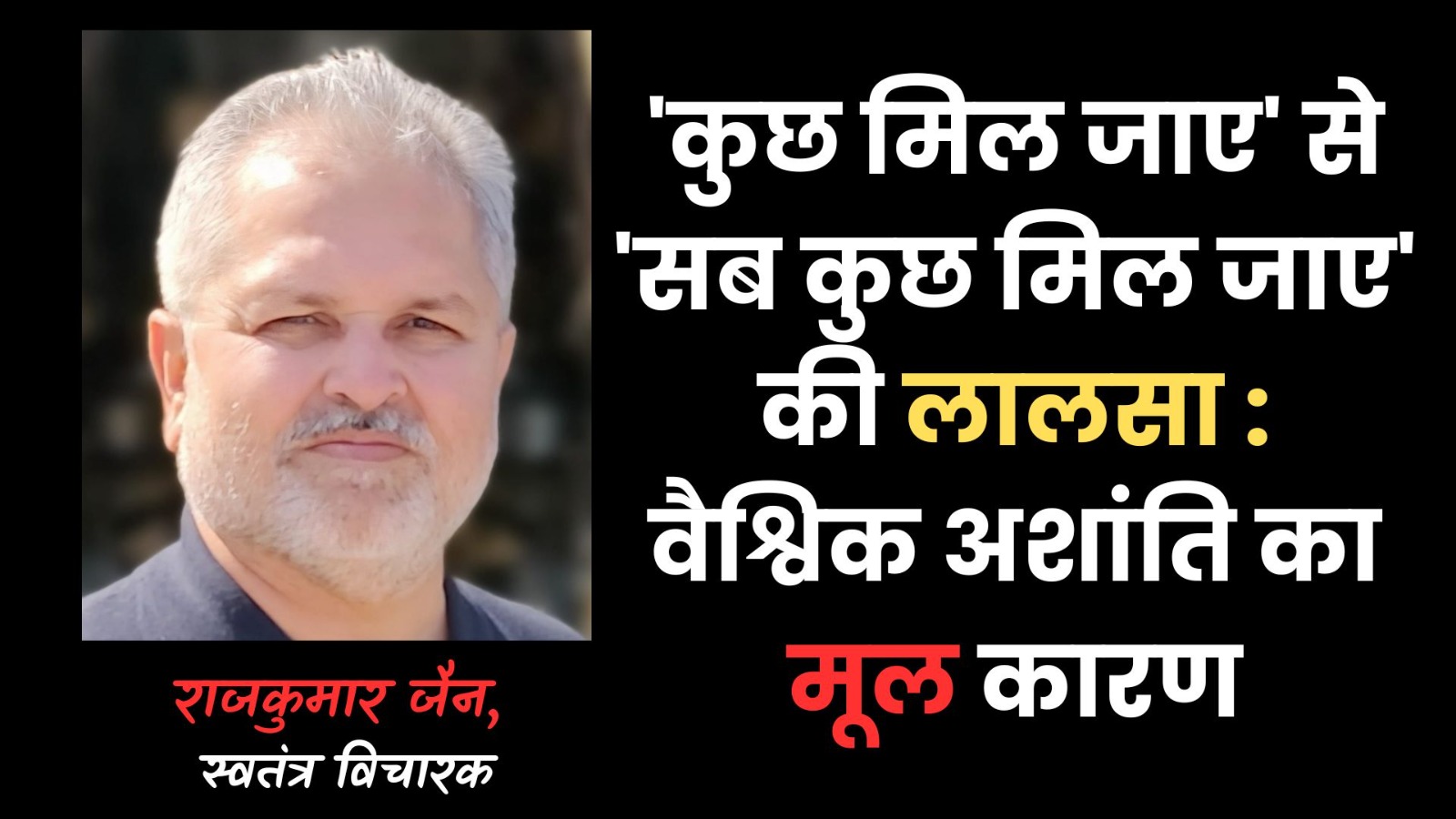(राजकुमार जैन, स्वतंत्र विचारक )- आज विश्व तकनीकी प्रगति और भौतिक समृद्धि के शिखर पर खड़ा है, लेकिन मानवीय चेतना भीतर से खंडित हो रही है, तकनीकी समृद्धि और मानसिक शांति के बीच की खाई दिनोंदिन गहरी होती जा रही है। राष्ट्रों के बीच संघर्ष, सामाजिक असमानता, पर्यावरणीय विनाश और व्यक्तिगत अवसाद की बढ़ती समस्याएं एक मौलिक प्रश्न उठाती हैं, क्या हमारी प्रगति की दिशा सही है। भारतीय दर्शन की शाश्वत परंपरा इस जटिल समस्या का एक गहरा और व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करती है – तृष्णा से मुक्ति के माध्यम से वैश्विक शांति का मार्ग।
मानवीय अशांति का मूल कारण बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतरी तृष्णा यानि में अतृप्त इच्छा छिपा है। यह तृष्णा एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो व्यक्ति को निरंतर असंतुष्ट और बेचैन बनाए रखती है। जब हम गहराई से विचार करते हैं तो समझ आता है कि प्रत्येक व्यक्ति का बाहरी संसार उसके आंतरिक संसार का प्रतिबिंब मात्र है।यह वह अदृश्य जाल है जो मनुष्य को जीवनपर्यंत उलझाए रखता है और उसे सच्चे आनंद से वंचित करता है।
मनुष्य की जीवन यात्रा “कुछ मिल जाए” की सहज आकांक्षा से शुरू होती है। भोजन, वस्त्र, आवास जैसी बुनियादी आवश्यकताएं उसे कर्म करने की प्रेरणा देती हैं। परंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब ये आवश्यकताएं पूरी होने के बाद भी इच्छाओं का सिलसिला रुकता नहीं और “सब कुछ मिल जाए” की अंधी दौड़ शुरू हो जाती है। यह अनियंत्रित हवस मनुष्य को अपनी चेतना से दूर कर देती है। अब वह केवल कर्म नहीं करता, बल्कि अपनी तृष्णा को शांत करने के लिए कुकर्म का भी सहारा लेने लगता है। यह वह बिंदु है जहां व्यक्ति अपनी मानवीय गरिमा को भूलकर एक विनाशकारी प्रतिस्पर्धा में शामिल हो जाता है।
तृष्णा की सबसे घातक विशेषता यह है कि यह कभी संतुष्ट नहीं होती। यह एक अगाध कुएं के समान है जिसे भरने का प्रयास किया जाए तो वह और भी गहरा होता जाता है। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, तत्काल दूसरी इच्छा उसका स्थान ले लेती है। यह प्रक्रिया मृगतृष्णा के समान है – रेगिस्तान में प्यासा व्यक्ति जल की तलाश में दौड़ता रहता है, लेकिन जल हमेशा उसकी पहुंच से दूर रहता है।
आधुनिक मनोविज्ञान भी इस सत्य को स्वीकार करता है कि मानसिक संतुष्टि बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन से आती है। जब व्यक्ति इस निरंतर चलने वाली दौड़ में फंस जाता है, तो वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। उसका मन हमेशा भविष्य की काल्पनिक संभावनाओं में उलझा रहता है। जब समाज का प्रत्येक सदस्य केवल अपनी तृष्णा की पूर्ति में लीन होता है, तो संघर्ष, असमानता और अन्याय का जन्म होता है। राष्ट्रों के बीच संसाधनों के लिए संघर्ष, आर्थिक असमानता, पर्यावरणीय विनाश और सामाजिक अशांति के मूल में यही अतृप्त तृष्णा काम करती है।
आज के युग में हम देखते हैं कि व्यक्ति और राष्ट्र अपनी संकीर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों का अहित करने से नहीं हिचकिचाते। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन की उपेक्षा, और सामाजिक न्याय की अनदेखी – ये सभी समस्याएं मूलतः मानवीय तृष्णा से ही उत्पन्न होती हैं। तृष्णाजनित तनाव का प्रभाव केवल मानसिक स्वास्थ्य पर नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। निरंतर चिंता, असंतोष और प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न तनाव आज महामारी का रूप ले चुका है। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अनिद्रा और अवसाद जैसी समस्याएं प्रत्यक्ष रूप से तृष्णाजनित तनाव से जुड़ी हैं।
भारतीय दर्शन केवल समस्या की पहचान नहीं करता, बल्कि उसका स्थायी समाधान भी प्रस्तुत करता है। सार यह है कि शांति किसी संस्था द्वारा नहीं, किसी राजनीतिक व्यवस्था द्वारा नहीं, बल्कि व्यक्ति की मानसिक अवस्था से उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति “स्व से पर” की ओर बढ़ता है, जब वह अपने व्यक्तिगत लाभ से महानतर उद्देश्य की ओर जाता है, तभी वह वास्तव में संतोष का अनुभव करता है और वहीं से विश्वशांति की नींव पड़ती है।
यहाँ समझना आवश्यक है कि संतोष का अर्थ निष्क्रियता या महत्वाकांक्षा का त्याग नहीं है। संतोष एक ऐसी उच्च मानसिक अवस्था है जहां व्यक्ति अपनी इच्छाओं का स्वामी बनता है, न कि उनका दास। संतोष की अवस्था में व्यक्ति परिणाम से अपनी खुशी को जोड़ता नहीं बल्कि “निष्काम कर्म” की भावना से कार्य करता है – पूर्ण समर्पण के साथ कर्म करता है परंतु फल की चिंता नहीं करता।
संतोष की प्राप्ति का प्रथम चरण आत्म-चिंतन है। जब तक हम अपनी इच्छाओं के मूल कारणों को नहीं समझेंगे, तब तक उन पर नियंत्रण पाना असंभव है। नियमित ध्यान, स्वाध्याय और आत्म-निरीक्षण हमें अपने मन की गहराई में जाने और अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को पहचानने में सहायता करता है।
कृतज्ञता संतोष की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम अपने पास उपलब्ध वस्तुओं, संबंधों और अनुभवों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो हमारा ध्यान “जो नहीं है” से हटकर “जो है” पर केंद्रित हो जाता है। यह दृष्टिकोण हमें अभाव की भावना से मुक्त करता है और पूर्णता की अनुभूति जगाता है।
भारतीय दर्शन “अपरिग्रह” के सिद्धांत पर बल देता है। इसका अर्थ है आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। जब हम सीमित उपभोग का सिद्धांत अपनाते हैं, तो हमें यह समझ आता है कि वास्तविक खुशी वस्तुओं के संग्रह में नहीं, बल्कि अनुभवों की गुणवत्ता में निहित है।
आज के वैश्विक परिदृश्य में जब तकनीकी प्रगति ने मानवीय संपर्क को कम कर दिया है, सामाजिक माध्यमों ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है और उपभोक्ता संस्कृति ने तृष्णा को भड़काया है, तब भारतीय दर्शन का यह संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है।
स्वार्थ की संकीर्ण दीवारों से बाहर निकलना संतोष की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। सेवा और परोपकार का भाव हमें व्यापक मानवता से जोड़ता है और आंतरिक संतुष्टि प्रदान करता है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तो हमें एक गहरी प्रसन्नता मिलती है जो किसी भी भौतिक उपलब्धि से कहीं अधिक स्थायी होती है।
जब व्यक्ति संतोष की अवस्था में होता है, तो उसकी यह मानसिक दशा समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। संतुष्ट व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में नहीं, बल्कि सहयोग में विश्वास करता है। वह दूसरों को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि सहयात्री मानता है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से संघर्ष कम होंगे, सहयोग बढ़ेगा और शांति स्थापित होगी। यह केवल एक आदर्शवादी सोच नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक संभावना है जिसे इतिहास में अनेक बार देखा गया है।
भारतीय दर्शन का यह शाश्वत सत्य आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पूर्व था। तृष्णा से मुक्ति का यह मार्ग कोई अंतिम गंतव्य नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। इस यात्रा में उतार-चढ़ाव स्वाभाविक हैं, लेकिन संतोष की दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम हमें अधिक शांति, अधिक प्रसन्नता और अधिक मानवीय करुणा की ओर ले जाता है।
वैश्विक शांति के लिए आवश्यक है कि संतोष के सिद्धांतों को शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया जाए। बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुष्टि में है। उन्हें कृतज्ञता, सहयोग और सेवा के मूल्य सिखाने चाहिए। सतत विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय संरक्षण जैसी अवधारणाएं वास्तव में संतोष के सिद्धांत से ही निकलती हैं।
वैश्विक शांति की स्थापना केवल राजनीतिक संधियों या आर्थिक समझौतों से नहीं हो सकती। इसके लिए आवश्यक है मानवीय चेतना में एक आमूल परिवर्तन। यह परिवर्तन तभी संभव है जब हम समझ लें कि सच्ची खुशी और शांति हमारी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की मानसिक अवस्था में निहित है। यह वह अवस्था है जहां हमारी इच्छाएं हमें संचालित नहीं करतीं, बल्कि हम अपनी इच्छाओं के स्वामी होते हैं। यही भारतीय दर्शन का सार है और यही आधुनिक मानवता के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश है।
इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जीवन में अपनाकर हम न केवल अपनी व्यक्तिगत अशांति से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि एक शांतिपूर्ण और न्यायसंगत विश्व के निर्माण में भी योगदान दे सकते हैं। यह एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को आत्मिक उन्नति से लेकर वैश्विक कल्याण तक ले जाता है।
आज जब विश्व अनेक संकटों से घिरा है, तब भारतीय दर्शन का यह संदेश एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो मानवता को सही दिशा दिखाता है। यह दिशा है संतोष की, शांति की, और सर्वकल्याण की।